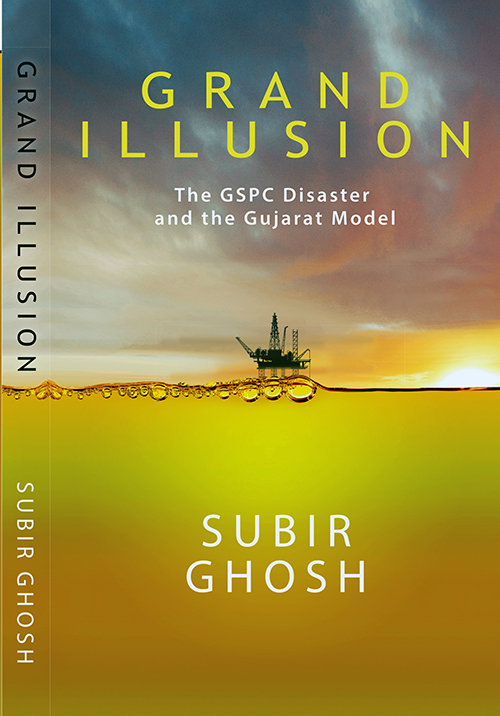यह देखना आश्चर्यजनक लगता है कि ऐतिहासिक जनसमर्थन से सत्ता में आई मोदी सरकार कितनी तेजी से अपना आधार गंवाती जा रही है। महज 15 माह पहले मई 2014 में 31.5 प्रतिशत पॉपुलर वोट के साथ यह सरकार सत्ता में आई थी। इसके बावजूद कॉर्पोरेट जगत की कद्दावर हस्तियों, दक्षिणपंथी चिंतकों, स्तंभकारों, बुद्धिजीवियों, जिनमें से कइयों ने मोदी सरकार में भरोसा जताया था और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया था, आज उनमें ही जैसे सरकार की कार्यप्रणाली और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्वक्षमता की आलोचना करने की होड़ लगी हुई है।
सरकार के प्रति इतनी जल्दी अगर मोहभंग की स्थिति बन गई है तो एक अर्थ में उसकी वजह स्वयं मोदी द्वारा जगाई गई आसमानी उम्मीदें भी हैं। चुनावों से पहले प्रचार अभियान के दौरान मोदी द्वारा जगाई गई यथार्थ-अयथार्थ उम्मीदों ने मतदाताओं को मानो सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। मोदी के 'मिनिमम गवर्नमेंट मैग्जिमम गवर्नेंस" के नारे ने तब देशवासियों को बहुत आकृष्ट किया था। लोग यह उम्मीद करने लगे थे कि अब केंद्र सरकार की अर्थनीतियों में एक तीखा दक्षिणपंथी मोड़ नजर आएगा। वे इस बात को भूल गए कि भारत जैसे देश में किसी भी सरकार के लिए बिजनेस-फ्रेंडली नीतियों का सूत्रपात करना बेहद मुश्किल है।
मायूसी की एक वजह यह भी है कि भारत में निवेश उस तेजी से नहीं आया है, जैसा कि मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद आने की उम्मीद की जा रही थी। इस कारण रोजगार-निर्माण की गति भी सुस्त रही है। वह तो गनीमत है कि मोदी सरकार के प्रारंभिक दिनों में ही कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में नाटकीय गिरावट की परिघटना दर्ज की गई, जिसके चलते महंगाई की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अगर ऐसा न होता तो मोदी सरकार के प्रति मोहभंग की स्थिति कहीं पहले से निर्मित होने लग जाती।
लेकिन कहानी केवल इतनी ही नहीं है। 27 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का यह कहते हुए मजाक उड़ाया था कि यह कार्यक्रम यूपीए सरकार की विफलताओं का 'स्मारक" है। इसके बावजूद जुलाई की आखिरी तारीख को मोदी सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 40882 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त व्यय के लिए संसदीय सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। इस राशि का एक-तिहाई हिस्सा उन्हीं योजनाओं के लिए है, जिन्हें भाजपा समय-समय पर अनुपयोगी बताकर निरस्त करती रही है। इनमें मनरेगा के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1975 में प्रारंभ की गई एकीकृत बाल विकास योजना भी शामिल है।
संकेत स्पष्ट हैं। भारत में कोई भी सरकार, फिर चाहे वह कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही हो या भाजपा के नेतृत्व में, ग्रामीण गरीबों के लिए संचालित की जाने वाली लोक-कल्याणकारी योजनाओं में कतरब्यौंत नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि इन योजनाओं के लिए जारी की जाने वाली राशि हितग्राहियों तक न पहुंचकर बीच में ही मध्यस्थों द्वारा हजम कर ली जाती है। ऐसे में लोक-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रणाली सुधारना एक बात है और उन्हें समाप्त कर देना दूसरी। लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाले खर्च में कटौती के प्रयास यदि प्रतीकात्मक हों, तो भी उसकेसियासी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सरकार यह देर से समझी।
गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और उनके परामर्शदाता समूह द्वारा योजना आयोग को नेहरूवादी-समाजवादी अतीत का भग्नावशेष बताकर मुस्तैदी से खारिज कर दिया गया था। उसके स्थान पर नीति आयोग बनाकर दक्षिणपंथी अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया को उसकी कमान सौंपी गई। नीति आयोग बने एक साल होने आया, लेकिन अभी तक योजना भवन की कार्यप्रणाली में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं देखा गया है। योजना भवन का नाम तक नहीं बदला जा सका है।
सरकार और उसके समर्थकों को अब तक यह समझ आ गया होगा कि विभिन्न् योजनाओं (जैसे कि जन-धन और स्वच्छ भारत) का नाम बदलकर और उनकी री-पैकेजिंग कर पुन: लोकार्पित कर देने भर से बुनियादी बदलाव नहीं आने वाले और जमीनी अमल का कोई विकल्प नहीं हो सकता। नए बैंक खाते खुलवाने का लक्ष्य अर्जित कर लेना एक बात है और उन खातों में पैसा जमा हो, यह सुनिश्चित करवाना दूसरी बात। टॉयलेट बनवाना एक बात है, उनका दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित कराना दूसरी बात।
कॉर्पोरेट इंडिया के मुखर प्रवक्ताओं में से एक राहुल बजाज ने हाल ही में एक टीवी चैनल पर कहा, '27 अगस्त 2014 को हमने एक सम्राट को देखा था। पिछले 20-30 सालों में दुनिया में बहुत कम ऐसे देश थे, जिनमें किसी नेता को इतना व्यापक जनादेश मिला हो। मैं इस सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सच तो यही है कि सरकार की चमक अब उतरने लगी है।"
सरकार के अपयश में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर उसके डावांडोल रवैये की भी अहम भूमिका रही। प्रतिष्ठित स्तंभकार स्वामीनाथन अंकलेसरिया अय्यर लिखते हैं कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मामले पर सरकार के ताजा रुख से यह स्पष्ट हुआ है कि वह अनिर्णय से ग्रस्त है और उसमें साहस का अभाव है। वह लड़ने के बजाय पीछे हटने को तैयार हो गई है। और यह कोई इकलौता मामला नहीं है। सरकार ने एकाधिक अवसरों पर एक पुख्ता रणनीति बनाने के बजाय एक कामचलाऊ कार्यनीति से ही संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति दर्शाई है। वहीं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष प्रतापभानु मेहता कहते हैं कि मोदी के इर्दगिर्द नेतृत्वशीलता का जो आभामंडल निर्मित किया गया था, वह अब छिन्न्-भिन्न् हो रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि उनकी सरकार राजनीतिक साहस का परिचय देगी, लेकिन उसके स्थान पर भ्रम और अनिश्चय का मंजर है।
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की शक्तियों में कटौती करने का अनमना प्रयास किया था और फिर जल्द ही सरकार ने अपने हाथ भी खींच लिए। नए आयकर रिटर्न फॉर्म को लेकर भी वित्त मंत्रालय इसी तरह कदम आगे बढ़ाकर पीछे हट चुका है। यह तो खैर अब जगजाहिर है कि नई दिल्ली में सत्ता कुछ ही लोगों में केंद्रीयकृत है। लेकिन इसके बावजूद सत्ता के गलियारों में भीषण खामोशी व्याप्त है। निश्चित ही, मोदी के लिए गुजरात में सरकार चलाना जितना आसान था, भारत में सरकार चलाना उतना आसान साबित नहीं हो रहा है और अफसोस कि गुजरात और भारत की सरकार चलाने के इस व्यापक अंतर को समझने की कोशिश भी नहीं की जा रही। आश्चर्य नहीं कि ऐसे में प्रधानमंत्री के विश्वस्त समर्थक भी मायूस हो रहे हैं। देखना होगा कि इस बार 15 अगस्त को मोदी लालकिले की प्राचीर से क्या घोषणाएं करते हैं।