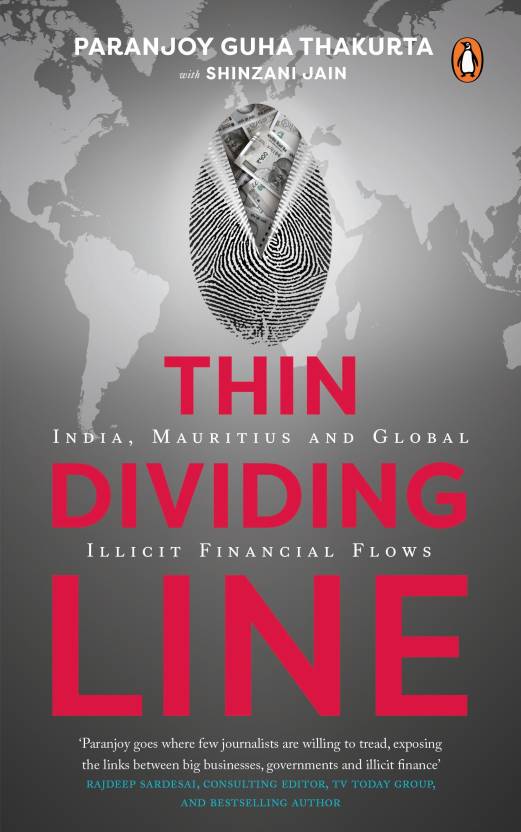यह तो खैर पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि संसद का मानसून सत्र न केवल हंगामाखेज रहेगा, बल्कि वह पूरी तरह से 'धुल" भी सकता है। अब जब ऐसा वस्तुत: होता नजर आ रहा है तो यह किसी के लिए भी अप्रत्याशित नहीं है। सवाल यही था कि क्या इसके बाद मोदी सरकार अपनी नीतियों में बुनियादी बदलाव लाने को मजबूर होगी। संसद में विधायी कार्य ठप हो जाने से सरकार के लिए मतदाताओं से किए गए वादों को पूरा करना निरंतर मुश्किल होता जा रहा है और इससे उस पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। उसके सामने बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की चुनौती भी मुंह बाए खड़ी है। सोमवार को सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अपने आग्रहों से पीछे हटने की जो तैयारी दिखाई, उसका तात्कालिक कारण भी यही हो सकता है।
जब यूपीए सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में, तब भाजपा द्वारा भी संसद की कार्यवाही ठप करने की ऐसी ही रणनीति का सहारा लिया गया था, लेकिन उसमें एक बुनियादी अंतर था। अपने दस वर्षीय कार्यकाल के अंतिम दौर में यूपीए सरकार उत्तरोत्तर अलोकप्रिय होती जा रही थी, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक लोकप्रिय बहुमत प्राप्त कर सत्ता में आई है और उस पर जनअपेक्षाओं का दबाव अपने दूसरे कार्यकाल वाली यूपीए सरकार की तुलना में कहीं अधिक है। माना जा सकता है कि अब सरकार पर इस दबाव के लक्षण नजर आने लगे हैं।
क्या भाजपा अपनी आर्थिक-सामाजिक नीतियों में बदलाव करने के लिए पहले से अधिक तत्पर रहेगी? आगामी तीन महीनों में जब देश की राजनीति का रुख धीरे-धीरे दिल्ली से बिहार की ओर शिफ्ट होगा, तो शायद इस सवाल का जवाब भी हमें मिलने लगे। यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे जदयू-राजद गठबंधन को भाजपा बिहार में हरा देती है तो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक और भी उत्साहित हो जाएंगे। लेकिन अगर भाजपा बिहार की लड़ाई हार जाती है तो यह न केवल दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद उसकी लगातार दूसरी बड़ी शिकस्त होगी, बल्कि बहुत संभव है कि इसके बाद उसे अपनी दक्षिणपंथी, कॉर्पोरेट-फ्रेंडली नीतियों में बदलाव लाते हुए अधिक लोकलुभावन नीतियों को अपनाने पर मजबूर होना पड़े।
संकेत अभी से नजर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को अब लगने लगा है कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत के बावजूद उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में वांछित बदलाव करने में सफल नहीं हो पाएगी। वे इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कहीं उनकी सरकार पर 'किसान-विरोधी" और 'गरीब-विरोधी" होने का ठप्पा न लग जाए, क्योंकि भारत की राजनीति में इस तरह का कोई ठप्पा पार्टी के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है।
बड़े मजे की बात है कि देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस, जो कि चुनावों में 50 प्रतिशत लोकप्रिय वोट हासिल करती हैं, की आर्थिक नीतियां कमोबेश एक जैसी ही रही हैं। और अगर भाजपा बिहार में चुनाव हार गई तो यह लगभग तय है कि दोनों पार्टियों की आर्थिक नीतियां और भी समान नजर आने लगेंगी।
लेकिन क्या यही बात भाजपा की सामाजिक नीतियों के बारे में भी कही जा सकेगी, क्योंकि इस बिंदु पर भाजपा और कांग्रेस में पर्याप्त अंतर हैं। बहुत संभव है कि संसद के निरंतर ठप रहने से निर्मित हुए राजनीतिक दबाव और राज्यों में चुनावी हार के बाद भाजपा को न केवल अपनी आर्थिक नीतियों में वाम के प्रति झुकाव रखने वाले कार्यक्रम बनाने को मजबूर होना पड़े, बल्कि उसे अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर भी पुनर्विचार करने को मजबूर होना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक संघ परिवार से जुड़े व अन्य लोगों द्वारा कही जा रही बातों पर यथासंभव मौन ही साध रखा है और स्वयं की एक अधिक 'समावेशी" छवि विकसित करने की कोशिश की है, लेकिन आने वाले समय में वे संघ के सामाजिक एजेंडे को आगे बढ़ाने को लेकर भी संकोच कर सकते हैं।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से प्रधानमंत्री मोदी के संबंध बहुत मधुर नहीं रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने ललितगेट मामले में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उनकी यही स्थिति राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबंध में भी है। विपक्ष ने इन तीनों के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद को ठप कर रखा है, वहीं इससे सरकार की साफ छवि को भी ठेस पहुंची है। खासतौर पर मध्यप्रदेश के व्यापमं घोटाले ने युवाओं के हितचिंतक होने के भाजपा के दावे को खासी क्षति पहुंचाई है, जबकि यह वर्ग हाल के दिनों में भाजपा का प्रमुख आधार रहा है। इन मामलों में उनकी स्थिति अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसी बनती जा रही है।
मोदी सरकार मई 2019 तक सत्ता में है। तब तक हालात में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है और आएगा भी। हाल ही में अपना 45वां जन्मदिन मनाने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है कि वे आक्रामक राजनीति की राह पर आगे बढ़ें। राहुल ने खुद ही यह रास्ता चुना है और वे फिलहाल लेफ्ट की भाषा बोल रहे हैं। एक अन्यमनस्क राजनेता और 'युवराज" के रूप में उनकी जो छवि निर्मित हो गई है, उसे बदलने और कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूती से खड़ा करने के लिए यह जरूरी भी है। देखना होगा कि वे कब तक जमीनी राजनीति की चुनौतियों को झेल सकेंगे। बिहार में उनके हस्तक्षेप के बाद ही लालू प्रसाद यादव पीछे हट गए थे। देखना होगा कि अब वे नीतीश कुमार की सराहना किन शब्दों में करते हैं। बिहार में उनके चुनाव प्रचार अभियान पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
2014 के लोकसभा चुनावों को भाजपा ने चतुराईपूर्वक अध्यक्षीय शैली के चुनावों की शक्ल दे दी थी। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी करार दे दिए गए उन चुनावों में मोदी ने शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन राजनीति को किसी पर्सनैलिटी कल्ट तक महदूद करना एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसके खतरे भी उतने ही हैं, जितने कि उसके फायदे। दिल्ली के चुनावों में यही देखने को मिला था।
बिहार के चुनावों में भी ऐसा हो सकता है, जहां जदयू-राजद गठबंधन ने तो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, वहीं भाजपा अभी तक ऊहापोह की स्थिति में बनी हुई है। दिल्ली में किरन बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद करारी हार झेल चुकी भाजपा अब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आधार पर ही बिहार में भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव के परिणामों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इससे न केवल देश के मौजूदा राजनीतिक रुख का पता लगेगा, बल्कि चुनावों के बाद यह भी साफ हो जाएगा कि केंद्र सरकार आने वाले समय में किस तरह की नीतियों को अख्तियार करेगी।