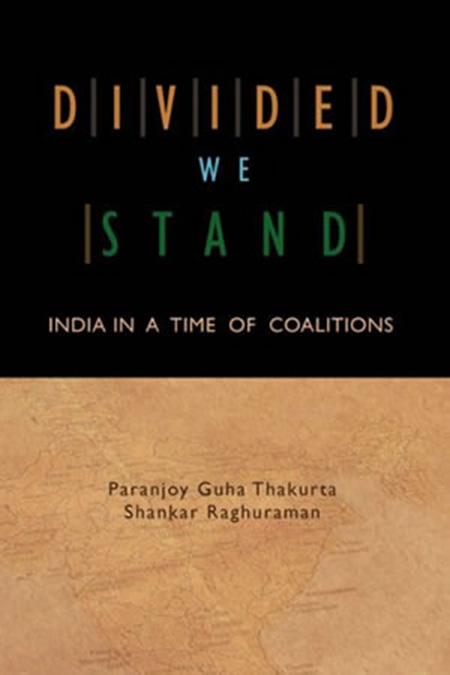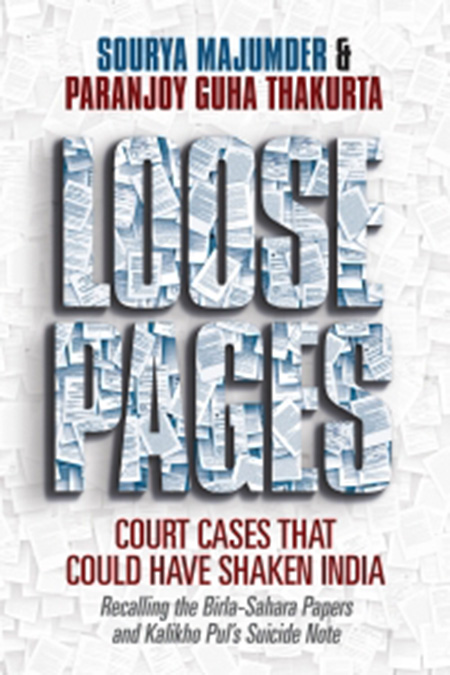बिहार चुनावों में हार के बाद भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसके सिवा कोई और विकल्प भी नहीं था कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति अधिक सौजन्य और सदाशयता का प्रदर्शन करें। उन्होंने ऐसा ही किया भी, जो कि संसद में प्रधानमंत्री के भाषण और फिर उसके बाद जीएसटी बिल पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को चाय पर बुलाने के उनके निर्णय से झलका। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि उनकी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के चंद व्यक्तियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, जिन्हें कि दिल्ली और बिहार के महत्वपूर्ण चुनावों में भाजपा की हार का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है?
वास्तव में भाजपा को लेकर उसके राजनीतिक विरोधियों में हमेशा से यह भ्रम की स्थिति रही है कि उसका चेहरा क्या है और मुखौटा क्या है। लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा को 'पार्टी विद अ डिफरेंस" बताया था। आज यही पार्टी अपने विचारधारागत और प्रयोजनमूलक 'डिफरेंसेस" (मतवैभिन्न्यों) को लेकर जूझती हुई लग रही है। बिहार चुनावों के दौरान और उसके बाद आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा के साथ ही अरुण शौरी, गोविंदाचार्य, शत्रुघ्न सिन्हा आदि ने जिस तरह की बातें कहीं, उन्हें चाहे या तो चंद 'एंग्री ओल्ड मेन" या फिर कुछ 'सत्तावंचितों" की खीझ और निराशा का प्रदर्शन मान लिया जाए, लेकिन नेतृत्व की जवाबदेही का जो सवाल उन्होंने उठाया, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ना ही इससे पार्टी में जाहिर होने वाली अंदरूनी कलह को नजरअंदाज किया जा सकता है। आने वाले समय में यह अंतर्कलह और कर्कश साबित हो सकती है, अगर जल्द ही संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया गया। क्या माना जाए कि मोदी के ताजा उदार रुख के बाद इसकी शुरुआत हो गई है?
बिहार चुनावों के बाद राज्यसभा में बहुमत पाने की भाजपा की उम्मीदें अब और धूमिल हो गई हैं। इसका सीधा-सीधा यह मतलब है कि संसद को चलाना है और जरूरी विधेयकों को पास करवाना है, तो भाजपा के नेताओं को विपक्ष से सार्थक संवाद करना होगा। इसके अलावा कोई और विकल्प उनके पास शायद नहीं रह गया है। यह एक विडंबना ही है कि कांग्रेस और वामदलों को सरकार की खासी राजनीतिक तवज्जो एक ऐसे समय में मिल सकती है या मिलने जा रही है, जब वे अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं और संख्याबल के लिहाज से तो सरकार पर अधिक दबाव बनाने की स्थिति में नहीं हैं।
संसद के उच्चतर सदन यानी राज्यसभा में सदस्यों का चयन और मनोनयन जिस अप्रत्यक्ष और पेचीदा तरीके से होता है, उसके मद्देनजर भी हालात में हाल-फिलहाल कोई बदलाव होता तो नजर नहीं आता। राज्यसभा के संख्याबल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुटकी लेते हुए उसे 'गैरनिर्वाचितों की बेरहमी" की संज्ञा दी थी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पास कराना सरकार अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण मान रही है और उसके समक्ष तात्कालिक चुनौती तो यही है कि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति कैसे निर्मित की जाए। इतना तो तय है कि अब तक जिस तरह से जेटली जीएसटी में सुधार के लिए विपक्षी नेताओं के सुझावों को खारिज करते आ रहे थे, वैसा शायद अब वे ना कर सकें।
हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर बिहार चुनावों में भाजपा की शानदार जीत हुई होती तो इस बात की कम ही संभावना थी कि मोदी सोनिया और मनमोहन को अपने यहां चाय और समोसों के लिए निमंत्रित करते। हां, यह जरूर संभव था कि संविधान पर चर्चा करते हुए वे तब भी संसद में इतना ही कुशल भाषण देते, जैसा कि उन्होंने दिया। लेकिन शायद बोलने का वक्त अब जा चुका है। मोदी के पास अब महज साढ़े तीन साल शेष हैं और यह तो तय है कि चुनावों से पहले उन्होंने देश से जितने वादे किए थे, उन सभी को वे पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि वे सत्ता में वापसी करना चाहते हैं तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वादों को तो उन्हें पूरा करना ही होगा। सत्ता में अपने अठारह महीनों में से पूरे ढाई महीने मोदी ने विदेश यात्राओं में बिताए हैं, लेकिन विदेश नीति का मतलब केवल एफडीआई और रॉक स्टार नुमा स्पीच ही नहीं होता। हमारे अपने पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरह से हाल के दिनों में भारत विरोधी भावनाएं देखने को मिली हैं, वे सरकार की विदेश नीति के लिए चिंता का सबब हो सकती हैं।
फिलवक्त, मोदी जलवायु परिवर्तन समिट में शिरकत करने पेरिस गए हैं, लेकिन देश लौटकर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि संसद में अपने भाषण के बाद सरकार की सदाशय छवि निर्मित करने की जो शुरुआत उन्होंने की है, उसमें वे कहां तक सफल रहेंगे। इसके लिए उन्हें संघ के सहयोग की खासी दरकार होगी। साथ ही उन्हें यह भी समझना होगा कि फिल्म और टीवी संस्थान, सेंसर बोर्ड इत्यादि में सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों से बुद्धिजीवियों में सरकार की मंशाओं और प्राथमिकताओं के प्रति जो संदेश गया है, उससे होने वाली क्षति का आकलन करें। ये अलग बात है कि भाजपा और बुद्धिजीवियों का एक-दूसरे के प्रति रवैया परंपरागत रूप से परस्पर वैरभाव और असहमति का ही रहा है।
भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की छवि अभी तक उजली बनी हुई है। यह सच है कि यूपीए सरकार के राज में हुए महाघोटालों से एनडीए सरकार ने अभी तक अपने को मुक्त रखा है, लेकिन यह भी सच है कि निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कालाबाजारी इत्यादि पहले की तरह बदस्तूर जारी हैं और आमजन में यही असंतोष जगाते हैं। राजनीति में सरकार के प्रति निर्मित होने वाली आम राय का बड़ा महत्व होता है। दादरी के बाद सरकार को यह भी समझ आ गया होगा कि देश के किसी कोने में घटित होने वाली कोई एक घटना भी अपने आशयों में इतनी असरकारी साबित हो सकती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता की विश्वसनीयता को प्रश्नांकित कर दे। इसके बाद राजनेताओं के समक्ष अमूमन खामोश रहने वाले पूंजीपतियों को भी कहने पर मजबूर होना पड़ा था कि सामाजिक समरसता का माहौल कायम किए बिना आर्थिक विकास भी नहीं किया जा सकता है।
हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में अपने भाषण के दौरान आपातकाल का उल्लेख किए बिना हिटलर के शासन से उसकी तुलना की थी। लेकिन यह भी याद रखा जाना चाहिए कि आपातकाल के समाप्त होने के बाद मतदाताओं ने एक लोकप्रिय सरकार को कैसे निरस्त कर दिया था। लोकतंत्र में जनादेशों से ही हवाओं के रुख का पता सबसे अच्छी तरह से चलता है।